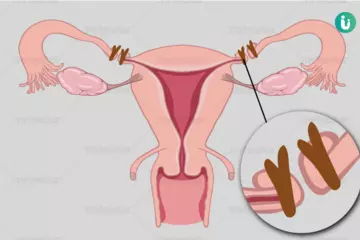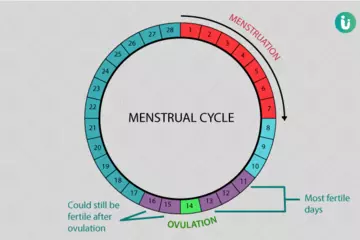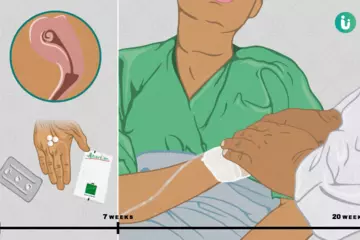मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर (एमआईडी) ऐसी स्थितियां हैं, जो आनुवंशिक व पर्यावरण या जीवन शैली कारकों के संयोजन के कारण विकसित होती हैं। इनमें शामिल हैं :
(1) दमा - Asthma in Hindi
दमा या अस्थमा में वायुमार्ग में सिकुड़न और सूजन आ जाती है और अतिरिक्त मात्रा में बलगम बनने लगता है।
दमा की पहचान
इलाज : अस्थमा के इलाज में स्टेरॉयड व एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा अस्थमा वाला इन्हेलर और नेब्यूलाइजर का भी प्रयोग किया जाता है।
(2) दिल की बीमारी - Heart disease in Hindi
हृदय को प्रभावित करने वाली किसी भी मेडिकल स्थिति को हार्ट डिजीज या दिल की बीमारी कहते हैं। इसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एनजाइना, कोरोनरी धमनी की बीमारी, अनियमित दिल की धड़कन, एथेरोस्क्लेरोसिस इत्यादि शामिल हैं।
दिल की बीमारी की पहचान
इलाज : दिल की बीमारी का इलाज इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर जीवनशैली में बदलाव, दवाइयां और मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी की मदद ली जाती है।
(3) डायबिटीज - Diabetes in Hindi
डायबिटीज तीन तरह की होती है - टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 में शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, टाइप 2 में इंसुलिन या तो बनता नहीं है या शरीर उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जबकि जेस्टेशनल डायबिटीज केवल गर्भावस्था के दौरान होता है और आमतौर पर यह डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है।
डायबिटीज की पहचान
इलाज : इसके इलाज में समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करना, जीवन शैली में बदलाव, स्वस्थ आहार लेना, इंसुलिन लेना व कुछ दवाएं (जैसे मेटफोर्मिन) लेना शामिल हैं।
डायबिटीज का इलाज:निरंतर जाँच करे,myUpchar Ayurveda Madhurodh डायबिटीज टैबलेट का उपयोग करे,स्वस्थ आहार ले, नियमित व्यायाम करे और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और सही दिशा में बढ़ें।
(4) सिजोफ्रेनिया - Schizophrenia in Hindi
यह एक ऐसा विकार है जो किसी व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और स्पष्ट रूप से व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
सिजोफ्रेनिया की पहचान
सिजोफ्रेनिया अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं :
- क्या बोलना है इस बारे में स्पष्ट न होना, जिसकी वजह से दूसरों को समझने में दिक्कत होती है
- चेहरे की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) में कमी
- भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी
- फोकस करने में कठिनाई
- मनोविकृति जैसे मतिभ्रम
इलाज : सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स, काउंसलिंग शामिल हैं।
(5) अल्जाइमर रोग - Alzheimer Disease in Hindi
अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है, जो धीरे-धीरे याद्दाश्त और सोच को नष्ट कर देता है और अंततः, सरल कार्यों को करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है।
अल्जाइमर रोग की पहचान
शुरुआती लक्षणों में चीजें खो देना, सामान्य दैनिक कार्यों को पूरा न कर पाना, फोकस न रहना मध्यम लक्षणों में करीबियों को पहचान न पाना, बिन बात क्रोधित होना, सोच और व्यवहार में बदलाव, जबकि गंभीर लक्षणों में दौरे पड़ना, त्वचा का संक्रमण, निगलने में कठिनाई इत्यादि शामिल हैं।
इलाज : इसके लिए कोई खास दवा नहीं है, लेकिन उपचार के तौर पर पीड़ित के मानसिक कार्य को बनाए रखना व व्यवहार संबंधी लक्षणों को नियंत्रित करना शामिल है।
(6) मल्टीपल स्क्लेरोसिस - Multiple Sclerosis in Hindi
यह एक क्रोनिक बीमारी है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और आंखों की नसों को प्रभावित करती है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक आवरण को नष्ट कर देती है। इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
(और पढ़ें - इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय)
मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पहचान
इलाज : मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज मौजूद नहीं है लेकिन उपचार का फोकस बीमारी की गति को धीमा करना और गंभीरता को कम करना होता है।
(और पढ़ें - थकान दूर करने के उपाय)

 आनुवंशिक विकार के डॉक्टर
आनुवंशिक विकार के डॉक्टर